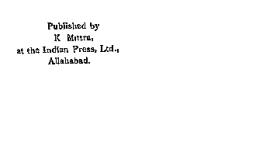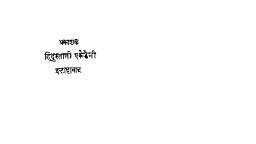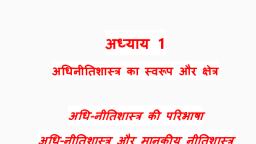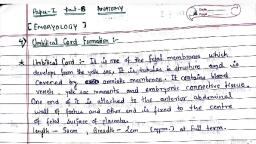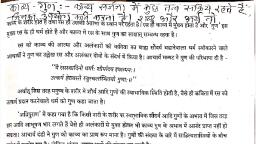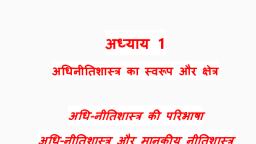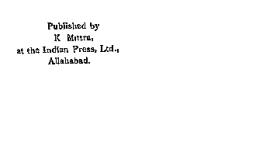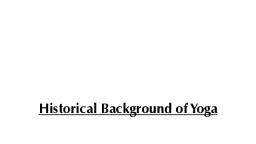Page 1 :
भारतीय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप, , प्रायः सभी मनुष्य यह दावा करेंगे कि उन्हें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान है और कि उन्हें इस तथ्य का भी ज्ञान, है। किन्तु जब हम ज्ञान की परिभाषा करने बैठते हैं तो पाते हैं कि हम अपने दावे के अर्थ अथवा स्वरूप के सम्बन्ध, में स्पष्ट नहीं हैं |, , वाचस्पति मिश्र ने भामती में ज्ञान का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जिससे अर्थ अथवा विषय प्रकाशित हो वह ज्ञान, है। (यो5यमर्थ प्रकाश: फलम् (भामती 1.1.4.)। किन्तु जब हम पूछते हैं कि 'प्रकाशित होने से क्या तात्पर्य है?', तो, इसके अतिरिक्त कि 'प्रकाशित करने' से अर्थ 'ज्ञान कराने' से है, हम कुछ नहीं कह सकते। वास्तव में ज्ञान एक सरल, प्रत्यय है तथा सभी सरल प्रत्ययों की भांति इसकी भी परिभाषा कर पाना कठिन है।, , ज्ञान के स्वरूप पर विचार करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 'ज्ञान' शब्द व्यापक तथा सीमित, दो अर्थों में प्रयुक्त होता है।, , व्यापक अर्थ में जहाँ भी चेतना का प्रकाश हो, वह ज्ञान कहलाता है। प्रत्येक चेतना-स्थिति इस दृष्टि से ज्ञानस्थिति है। इस दृष्टि से हमें स्वीकार करना होगा कि ज्ञान केवल मानव का एकाधिकार नहीं है वरन् पशुओं को भी, जान होता है। उच्च कोटि के प्राणियों में इस प्रकार के ज्ञान की संभावना में किसी को विशेष आपत्ति नहीं होगी।, किन्तु जब हम निम्न कोटि के प्राणियों, उदाहरणार्थ अमीबा आदि के विषय में सोचें तो कठिनाई का अनुभव होना, स्वाभाविक है। साथ ही, जब हम प्राणी वर्ग की निरन््तरता तथा तारतम्य को ध्यान में रखकर विचार करते हैं तो, कोई ऐसी रेखा नहीं दिखलाई देती है जहाँ से चेतना का प्रारम्भ स्वीकार किया जा सके। इतना ही नहीं, जब हम प्राणी, वर्ग तथा वनस्पति वर्ग पर भी दृष्टि डालते हैं तथा इसका स्पष्ट निर्णय करने में असफल रहते हैं कि वास्तव में कहाँ, से वनस्पति वर्ग की समाप्ति तथा प्राणि-वर्ग का प्रारम्भ स्वीकार किया जाये, तब हमारी कठिनाई और भी बढ़ जाती, है।, , हम देखते हैं कि कुछ वनस्पति वर्ग के तथा अमीबा आदि प्राणियों के व्यवहार में मूलभूत भिन्नता नहीं है। ऐसी, अवस्था में यह स्वीकार करना पड़ता है कि चेतना की इष्टि से भी वनस्पति से लेकर मनुष्य तक निरन्तर विकास, पाया जाता है। मानव में जो स्पष्ट चेतना है वह प्राणिवर्ग में निरन्तर धूमिल्र होती गई है तथा और अधिक धूमिल, तथा अव्यक्त रूप में यह वनस्पति वर्ग में भी अवश्य वर्तमान है।, , जैन दार्शनिकों ने इसी कारण वनस्पति वर्ग को भी सजीव द्रव्य स्वीकार किया है। चेतना जीव का अपरिहार्य गुण है, जो पुदूगल के आवरण से धूमित्र तो हो सकता है किन्तु उसका उसमें सर्वथा अभाव असंभव है। शंकर तथा श्री, अरविन्द आदि दार्शनिक चेतना की उपस्थिति सर्वत्र व्याप्त मानते हैं। श्री अरविन्द का कथन है कि जड़ पदार्थ भी, वास्तव में चेतन रूप ही है, यद्यपि चेतना वहाँ सुप्त स्थिति में होती है | शंकर भी चेतना के अभाव को किसी भी, स्थान पर असम्भव मानते हैं।, , सीमित अर्थ में ज्ञान सदैव एक निर्णय (जजमेंट) के रूप में होता है। इस दृष्टि से सविकल्पक चेतना ही ज्ञान की, कोटि में पाती है।
Page 2 :
ज्ञान के इन दोनों रूपों में स्तर-भेद ही माना जा सकता है, कोटि-भेद नहीं। दोनों एक दृष्टि से ज्ञान की ही अवस्थाएँ, हैं। अतः हम सामान्य रूप से ही इस विषय पर विचार करेंगे। वनस्पति तथा पशु वर्ग में चेतना का कया स्वरूप होता, है? तथा उनके ज्ञान का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है?, यह एक अलत्रग प्रश्न है तथा उस पर हम यहाँ, विचार नहीं करेंगे।, , ज्ञान के विषय में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि यह किस कोटि की सत्ता है? विभिन्न भारतीय, दार्शनिकों ने इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं तथा इस दृष्टि से वे चार मुख्य श्रेणियों में विभकत किये जा, सकते हैं।, , 1. कुछ दार्शनिक ज्ञान को गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे यह सिद्धान्त दो भागों में विभाजित किया जा, सकता है। प्रथम के अनुसार ज्ञान को आगन्तुक गुण के रूप में स्वीकार किया गया है तथा दूसरे के अनुसार इसे, अनिवार्य गुण के रूप में। ज्ञान को आगन्तुक गुण मानने वाले दार्शनिक फिर से दो शाखाओं में विभ्रक्त हो जाते हैं।, प्रथम चार्वाक दर्शन, जो ज्ञान को भौतिक तत्त्वों का ही आगन्तुक गुण स्वीकार करते हैं तथा दूसरे न्याय, वैशेषिक, तथा प्राआकर, जो ज्ञान के गुणी या धर्मी के लिए भौतिक तत्त्व को अपर्याप्त मानते हैं तथा इसीलिए उनका दावा है, कि ज्ञान के गुणी रूप में हमें एक अलग तत्त्व आत्मा को स्वीकार करना होगा। ज्ञान आत्मा का आगन्तुक गुण है,, भौतिक पदार्थों का नहीं। जो दार्शनिक ज्ञान को आत्मा का अनिवार्य गुण मानते हैं उनमें रामानुज, जैन आदि मुख्य, हैं।, , , , , , , , , , 2. इसके विपरीत भाट॒ट मीमांसकों का मत है कि ज्ञान आत्मा के गुण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।, , ज्ञान आत्मा का कार्य है, गुण नहीं। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा होता है तो वे इसे आत्मा में कर्म की, योग्यता अथवा शक्ति के रूप में स्वीकार करते है |, , 3. ज्ञान के विषय में तीसरा मत सांख्य तथा अद्वैत वेदान्त का है जो ज्ञान को गुण अथवा कर्म के रूप में स्वीकार, नहीं करते। उनके अनुसार जान स्वयं में द्रव्य है तथा किसी अन्य अधिष्ठान की उसे आवश्यकता नहीं है। योगाचार, दार्शनिक यद्यपि ज्ञान को द्रव्य कहना स्वीकार नहीं करते, किन्तु सामान्य अर्थ में वह गुण अथवा कर्म भी नहीं है।, उनके अनुसार ज्ञान को किसी अन्य अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इस इष्टि से योगाचार दर्शन सांख्य तथा, , अद्वैत मत के समान ही है।, , 4. ज्ञान के विषय में एक अन्य चौथे मत की चर्चा और की जा सकती है जो शून्यवादियों का है। यह मत उपर्युक्त, सभी मतों से भिन्न है। ये दार्शनिक ज्ञान को उपर्युक्त अथवा किसी भी अन्य कोटि में रखने को सहमत नहीं हैं। इस, मत को हम शून्यवादी मत कह सकते हैं। अब हम इन मतों का विस्तृत वर्णन करेंगे।, , , , 10100/244९ 45 9५०11५ ०11९ 52/(॥४५०/०, दां01507 06 197176/014), , जानः एक आगन्तुक गुण के रुप में /चार्वाक मत?, , चार्वाक दार्शनिक पूर्णरूपेण भौतिकवादी हैं तथा वे किसी भी आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं।, ऐसी अवस्था में जो स्पष्ट कठिनाई उनके सामने आती है वह है ज्ञान की व्याख्या करना। आत्मा, ईश्वर आदि, आध्यात्मिक सत्ताओं का तो वे इस आधार पर खंडन कर सकते हैं कि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता तथा प्रत्यक्ष के, अतिरिक्त सभी प्रमाण वास्तव में प्रमाण नहीं हैं, किन्तु ज्ञान का खंडन इस तर्क के आधार पर नहीं हो सकता,
Page 3 :
क्योंकि ज्ञान की सत्ता तो उन्हें भी अवश्य ही माननी होगी। चार्वाक ज्ञान की व्याख्या भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में ही, करते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान के लिए किसी आध्यात्मिक तत्त्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान भौतिक, वस्तुओं का उसी प्रकार का गुण है जिस प्रकार रंग, रूप आदि उनके गुण हैं। उनका कहना है कि यह बात सही है, कि ज्ञान किसी भूत विशेष में हमें दिखलाई नहीं देता, कुछ शरीर विशेषों में ही ज्ञान का उदय होता है, किन्तु जिस, प्रकार मादक द्रव्यों से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार भौतिक पदार्थों के देह के रूप में परिणत हो जाने, पर इन्हीं तत्त्वों में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है।(तेभ्य एव देहाकार परिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवच्चैतनन््यमुपजायते।, तेषु विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनष्यति। सर्व दर्शन संग्रह।) भौतिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर शरीर रूप, में एकत्रित होते हैं तो उनमें ज्ञान रूपी एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भौतिक पदार्थों का, आगन्तुक गुण है। जब ये भूत विघटित होते हैं तो उनमें चैतन्य का यह गुण भी समाप्त हो जाता है।, , अपने मत के पक्ष में चार्वाक दार्शनिकों का एक मुख्य तर्क यह है कि यदि पृथ्वी आदि चतुर्भूतों से किसी चैतन्य की, अभिव्यक्ति नहीं होती तो सोकर उठने वाले व्यक्ति में यह चैतन्य-शक्ति कहाँ से आ जाती है? सोने के समय से पूर्व, तो चैतन्य शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि शरीर और चैतन्य का कोई सम्बन्ध नहीं है तो शरीर में विकार उत्पन्न होने, से चेतना में विकृति क्यों हो जाती है ?, , आलोचना, 'चैतन्य शरीर का गुण है' इस चार्वाक मत की विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने कट्रु आलोचना की है।, , 1. वात्स्यायन का कथन है कि यद्यपि चैतन्य शरीर में ही इष्टिगत होता है किन्तु केवल इसीलिए इसे शरीर का गुण, नहीं माना जा सकता। द्रवता तथा उष्णता दोनों जल में विद्यमान होते हैं किन्तु जबकि द्रवता जल का अपना गुण, है, उष्णता जल का गुण न होकर अग्नि का गुण है।, , 2 चैतन्य शरीर का उसी प्रकार गुण नहीं माना जा सकता जिस प्रकार रूप उसका गुण है। रूप शरीर में सदैव वर्तमान, होता है। मृत्यु होने पर भी रूप का शरीर में प्रभाव नहीं होता किन्तु चैतन्य का निद्रा, मूर्छा तथा मृत्यु के समय, अभाव हो जाता है।, , 3. चेतना समस्त शरीर में व्याप्त होती है। शरीर विभिन्न अंगों वाल्रा होता है तथा इस प्रकार प्रत्येक अंग को अलग, चेतन माना जाना चाहिए। किन्तु शरीर के विभिन्न अंगों को अलग-अलग रूप से चेतन नहीं माना जा सकता।, , 4. शरीर के गुणों का या तो बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान हो सकता है अथवा फिर उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ज्ञान न, तो इन्द्रियों से ज्ञात होता है और न ही वह अप्रत्यक्ष है। उसका बोध वास्तव में मन के द्वारा होता है तथा मन के, द्वारा शरीर के किसी गुण का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः चैतन्य शरीर से भिन्न अन्य तत्त्व (आत्मा) का गुण है।, (न्याय भाष्य ॥. 2. 46, 47, 50, 53; न्याय वार्तिक 1. 2. 55; न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ॥, 2, 51), , 5. उदयन का तर्क है कि यदि चैतन्य शरीर का गुण होता तो बचपन में किये गये अनुभवों का युवावस्था में स्मरण, नहीं हो सकता था। शरीर में परिवर्तन होता रहता है। उसका विकास तथा क्षय होता है तथा युवावस्था में वही शरीर, नहीं रहता जो बचपन में था। वह इससे भिन्न होता है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार चैत्र के द्वारा किये गए अनुभवों, का मैत्र को स्मरण नहीं हो सकता उसी प्रकार बचपन में किये गए अनुभव युवावस्था में याद नहीं रहने चाहिये।, किन्तु ऐसा होता नहीं है। हमें बचपन की स्मृति रहती है। इसीलिए शरीर से भिन्न आत्मा को मानने की आवश्यकता
Page 4 :
है जिसका गुण यह चैतन्य है। यदि यहाँ चार्वाक दार्शनिक यह कहें कि पूर्व शरीर का ज्ञान शरीरगत वासना अथवा, संस्कारों के पूर्व शरीर से उत्तर शरीर में चले जाने (वासना संक्रमण) के कारण होता है। तो उदयन कहते हैं कि तब, तो माता को हुए ज्ञान का संतान को स्मरण होना चाहिए, क्योंकि माता के शरीर से ही संतान के शरीर की उत्पत्ति, होती है। यदि यह कहा जाए कि संस्कारों का रक्षण इसीलिए होता है कि पूर्व शरीर उपादान कारण है, तो यह भी, युक्त नहीं है, क्योंकि हाथ के शरीर से अलग हो जाने पर हाथ के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया गया था उसका, स्मरण नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि हाथ तो शरीर का उपादान कारण नहीं है। न ही चार्वाक यह कह सकते हैं कि, अणु नित्य हैं तथा उन परमाणुओं के कारण ज्ञान का शरीर में रक्षण होता है, क्योंकि परमाणु अद्दश्य होते हैं तथा, यदि ज्ञान परमाणुओं का गुण होता तो वह भी अद्ृश्य हो जाता । ((न्याय कुसुमांजलि, 1.15; न्याय कुसुमांजलि, मकरन्द 1.15), , जयन्त का भी कहना है कि दो अवस्थाओं में शरीर भिन्न-भिन्न होता है। ऐसी अवस्था में यदि चैतन्य को शरीर का, ही गुण माना जाये तो स्मृति की व्याख्या नहीं हो सकती। शरीर में वृद्धि तथा क्षय होता रहता है। अत: यदि चैतन्य, शरीर का ही गुण है तो इसके साथ-साथ चैतन्य में भी वृद्धि तथा क्षय होना चाहिए, जो नहीं होता।, , जान: एक आगन्तुक गुण के रुप में (न्याय, वैशेषिक तथा प्राआकर मीमांसक), , उपयुक्त तर्कों के आधार पर न्याय-वैशेषिक तथा प्राभाकर चैतन्य के अधिष्ठान अथवा धर्मी के रूप में शरीर से भिन्न, एक आध्यात्मिक तत्त्व को स्वीकार करना आवश्यक समझते हैं | यह तत्त्व आत्मा है किन्तु इतना होते हुए भी वे, चार्वाक दार्शनिकों के इस मत से सहमत हैं कि चैतन्य अपने धर्मी का आगन्तुक गुण है, अनिवार्य गुण नहीं। आत्मा, स्वयं में चेतन अथवा चैतन्यस्वरूप नहीं है। जब विषय, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के साथ आत्मा का संयोग होता, है तभी उसमें ज्ञान अथवा चैतन्य रूपी गुण की उत्पत्ति होती है। उनका कहना है कि यदि चैतन्य आत्मा का अनिवार्य, गुण होता तो उसमें इसका कभी भी प्रभाव नहीं हो सकता था। किन्तु हम प्रायः देखते हैं कि सुषुष्ति, मूर्छा आदि, अवस्थाओं में हम ज्ञान-शून्य होते हैं | इसका एकमात्र कारण यही है कि इस स्थिति में आत्मा का विषय आदि से, संयोग नहीं रहता और इससे आत्मा में चेतना का अभाव हो जाता है।, , न्याय, वैशेषिक तथा प्राभाकर मीमांसक अपने इस सुधार से एक ओर यह संतोष प्राप्त करते हैं कि ज्ञान के गुणी के, रूप में वे एक नित्य द्रव्य को स्वीकार कर उन सभी आलोचनाओं से मुक्ति पा जाते हैं जो कि चार्वाक दार्शनिकों के, विरुद्ध इसलिए की जा सकती हैं कि वे ज्ञान के आधार रूप में अनित्य तथा परिवर्तनशील शरीर को स्वीकार करते, हैं, और दूसरी ओर अपने मत में वे उन सब विशेषताओं को भी पाते हैं जिनके कारण चार्वाक मत अन्य दर्शनों से, अधिक तर्कयुक्त प्रतीत होता है। चार्वाक दार्शनिकों की भांति चेतना को आगन्तुक गुण स्वीकार कर वे इस प्रश्न से, बच जाते है कि यदि चेतना नित्य आत्मा का गुण है तो उसमें सुषुप्ति आदि के समय इसका अभाव क्यों होता है ?, , आलोचना, , किन्तु यदि वास्तव में देखा जाये तो न्याय मत उतना ही असंतोषप्रद सिद्ध होता है जितना कि चार्वाक मत। न्याय, मत का भारतीय दार्शनिक संदर्भ में सबसे अधिक दुर्बल पक्ष है आत्मा की स्वयं में चैतन््य-रहितता। यदि आत्मा स्वयं, में चेतना-शून्य है तब आत्मा के लिए अनुभव-प्रमाण संभव नहीं है। यद्यपि न्याय दर्शन में आत्मा का मानस प्रत्यक्ष, स्वीकार किया गया है, किन्तु उसकी यह अवधारणा अनेक तार्किक कठिनाइयों से ग्रस्त है। मन एक इन्द्रिय है तथा
Page 5 :
प्रत्यक्ष में इन्द्रिय का मुख्य कार्य विषय का आत्मा से सन्निकर्ष कराना है। ऐसी अवस्था में आत्मा से आत्मा का, सन्निकर्ष कराने के लिए एक अन्य माध्यम मन की आवश्यकता हो, यह उचित नहीं जान पड़ता | साथ ही मुक्तावस्था, में तो, जबकि आत्मा का मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि से पूर्ण रूपेण सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है तब आत्मा का किसी, भी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान नितांत असंभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ अद्वैत वेदांत आदि दर्शनों में आत्मा, के लिए सबसे प्रबत्न प्रमाण अनुभव है, जिसे कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, वहाँ न्याय आदि मतों में आत्मा, का केवल चेतना के गुणी के रूप में अनुमान मात्र लगाया जा सकता है। चेतना को स्वयं में द्रव्य रूप न मान कर, उसे केवल गुण रूप ही क्यों स्वीकार किया जाये?, इसका न्याय के पास कोई उत्तर नहीं है। बौदधों ने प्रबल तर्क के, आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गुणों से भिन्न किसी स्वतन्त्र धर्मी अथवा गुणी को मानने का, कोई आधार नहीं है। न्याय मत के तर्क यहाँ पर बौदधों के तर्कों के सामने नहीं ठहरते हैं।, , दूसरे दार्शनिक, जो चेतना को आत्मा का गुण स्वीकार करते हुए भी उसे उसका अनिवार्य गुण कहते हैं, वे कह सकते, हैं कि नित्य चेतन आत्मा का अनुभव के द्वारा ज्ञान होता है तथा इस प्रकार इसकी सत्ता प्रमाणित होती है। किन्तु, न्याय दार्शनिक इस तर्क का सहारा भी नहीं ले सकते तथा इस प्रकार आधार रूप में आत्मा को स्थापित करते समय, वे अपने आपको बालू के टीले के ऊपर खड़ा पाते हैं, जिस पर टिके रहना उनके लिए कठिन हो जाता है।, , आत्मा जैसे नित्य द्रव्य को ज्ञान का आधार मान लेने पर न्याय आदि मत को लगता है जैसे उन्होंने स्मृति आदि, की व्याख्या सम्बन्धी समस्याओं को सुलझा लिया, जो चार्वाक दार्शनिकों के लिए कठिन हो रहा था। किन्तु यदि, गंभीरता से विचार करें तो ल्रगता है कि वे यहाँ पर भी सफत्रता प्राप्त नहीं कर सके। किसी भी द्रव्य में जब कोई, गुण विशेष उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है तब उसका उसमें कया अवशेष रहता है ? कोई वस्त्र अभी सफेद है, इसके, पश्चात् इसको काला रंग लिया गया। अब प्रश्न है, क्या अब भी वह सफेद रंग उस वस्त्र में किसी न किसी रूप में, सुरक्षित रहा हुआ कहा जा सकता है ? न्याय दर्शन असत् कार्यवादी है तथा वहाँ नई उत्पत्ति तथा नाश ही के लिए, स्थान है, आविर्भाव तथा तिरोभाव के लिए नहीं |।, , अतः इस प्रश्न के लिए उनका एकमात्र उत्तर हो सकता है कि काला रंग दे देने पर श्वेत रंग का नाम हो गया तथा, काले रंग की नई उत्पत्ति हुई। ऐसी स्थिति में एक ज्ञान विशेष एक समय-विशेष पर आत्मा-विशेष में उत्पन्न हुआ,, इसके पश्चात् वह नष्ट हो गया। तब न्याय मत से यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि नित्य आत्मा का गुण होने, से प्रातः सोकर उठने पर उस कल वाले ज्ञान का उदय उसमें फिर से हो जायेगा।, , वस्तुतः न्याय के अनुसार अनुभव के संस्कार आत्मा में रक्षित स्वीकार किये गए हैं। सभी संस्कार आत्मा में रहने, पर भी विशेष कारण की उपस्थिति में ही जागृत होते हैं सर्वदा नहीं। महर्षि गौतम ने प्रणिधान, निबन्ध, आभास आदि, पच्चीस हेतुओं की चर्चा अपने सूत्र ग्रन्थ में की है (3. 2. 41) किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है न्याय मत में ज्ञान, के अव्यक्त रूप में रक्षित रहकर पुनः व्यक्त होने की धारणा मान्य नहीं हो सकती। इस प्रकार स्मृति में उदित हुआ, ज्ञान पूर्ण रूपेण नवीन ज्ञान होगा।, , न्याय मत के विरुद्ध जो अन्य सामान्य आपत्ति है वह भी इस मत को दूषित करती है। न्याय के अनुसार आत्मा, विभु रूप है। तथा ऐसी अवस्था में उसका सम्पर्क सदैव सभी हेतुओं से रहना चाहिए। इससे आत्मा की सदैव ही, सर्वज़ता की स्थिति बनी रहनी चाहिए।